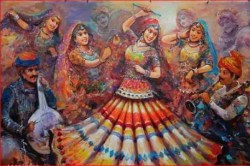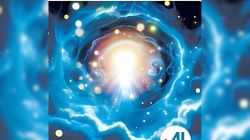Sunday, May 4, 2025
एआइ का दुरुपयोग : डिजिटल वाटरमार्किंग व मेटाडेटा टैगिंग की जरूरत
— नृपेन्द्र अभिषेक नृप
(स्वतंत्र लेखक एवं स्तंभकार)
जयपुर•May 03, 2025 / 12:36 pm•
विकास माथुर
आज के दौर में व्यक्ति स्वयं सोचने, लिखने या चित्रित करने के स्थान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के सहारे अपने विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं को आकार देने लगा है। चित्रकला हो या साहित्य-सृजन, संगीत हो या चलचित्र निर्माण, हर क्षेत्र में एआइ का दखल बढ़ता जा रहा है। लेकिन यह प्रगति तब भयावह रूप लेती है जब इसका दुरुपयोग समाज को भ्रमित करने, जनमत को प्रभावित करने और सच को झूठ में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है।
संबंधित खबरें
इस युग में जब विचार, संवेदना और कल्पना भी कृत्रिमता की चपेट में हैं, तब सबसे बड़ा संकट मनुष्य की आत्म-पहचान का है। मौलिकता केवल एक रचना की विशेषता नहीं, बल्कि व्यक्ति की चेतना का प्रतिबिम्ब होती है। यदि यह चेतना ही अब बाहरी उपकरणों के सहारे संचालित होने लगे, तो हम अपनी आत्मा से अपनी जड़ों से कटते चले जाएंगे। विचारणीय यह भी है कि जब हर चीज को मशीनें रचने लगेंगी, तब मनुष्य की भूमिका क्या केवल उपभोक्ता की रह जाएगी?
हाल में हैदराबाद विश्वविद्यालय के कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में बुलडोजर चलने की आड़ में जो वीडियो और तस्वीरें प्रचारित की गईं, उसमें काफी सारी एआइ जनित थीं और उनका उद्देश्य एक खास नैरेटिव गढऩा था। ऐसी घटनाएं केवल एक उदाहरण नहीं हैं बल्कि इस गंभीर संकट का संकेत हैं कि सत्य और असत्य अब एक जैसे दिखने लगे हैं। इस विकट परिस्थिति में यह जानना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि कोई तस्वीर, वीडियो या रचना वास्तव में मौलिक है या कृत्रिम। दुर्भाग्यवश आज भी आमजन के पास ऐसा कोई व्यापक और सार्वभौमिक साधन नहीं है, जिससे वह तत्काल पहचान सके कि किसी चित्र या वीडियो की उत्पत्ति कहां से हुई है?
हालांकि तकनीक के क्षेत्र में प्रयास प्रारंभ हो चुके हैं। अमरीका तथा यूरोपीय संघ में कुछ शोध संस्थान तथा निजी कंपनियां इस दिशा में ‘डिजिटल वाटरमार्किंग’ और ‘मेटाडेटा टैगिंग’ जैसी तकनीकों पर कार्य कर रहे हैं। यह तंत्र हर एआइ जनित सामग्री पर एक अदृश्य परंतु अटूट छाप छोड़ता है जिसे कोई आसानी से मिटा नहीं सकता। इस छाप को प्रमाण की भांति प्रयोग किया जा सकता है कि फलां चित्र या वीडियो किसी एआइ मॉडल द्वारा तैयार किया गया है। प्रसिद्ध एआइ कंपनियां जैसे ओपन एआइ, गूगल और मेटा इस विषय में अपनी जवाबदेही तय करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। वे अपने एआइ मॉडलों में एक ऐसा अंतर्निहित हस्ताक्षर जोडऩे पर विचार कर रही हैं, जो उपयोगकर्ता को बता सके कि सामग्री एआइ जनित है। भारत में इस दिशा में अभी जागरूकता की कमी है, परन्तु नीति निर्धारकों तथा तकनीकी विशेषज्ञों को अब इस संकट की गहराई समझनी चाहिए।
यदि समय रहते कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई, तो यह तकनीक लोकतंत्र, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती है। इसके लिए सरकार एक ऐसा सार्वभौमिक ऐप विकसित कर सकती है या अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से कोई ऐसा डिजिटल ढांचा तैयार किया जा सकता है, जिसमें किसी भी डिजिटल सामग्री को अपलोड कर उसकी मौलिकता की जांच की जा सके। आज ‘डीपफेक’ नामक तकनीक इतनी सशक्त हो चुकी है कि वह किसी व्यक्ति की आवाज, चेहरा और हावभाव की हूबहू नकल कर सकती है।
ऐसी परिस्थितियों में सत्य को पहचाना कठिन ही नहीं, असंभव प्रतीत होता है। इसलिए एआइ कंपनियों को एक ‘हॉलमार्क’ अथवा ‘डिजिटल पहचान चिह्न’ देना अनिवार्य किया जाना चाहिए, जो कानून द्वारा संरक्षित हो और जिसकी छेड़छाड़ दंडनीय हो। एक अन्य समाधान यह भी हो सकता है कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में डिजिटल साक्षरता के पाठ्यक्रम को अनिवार्य किया जाए, जिससे भावी पीढ़ी तकनीकी सृजन और वास्तविकता के भेद को समझ सके। यह ज्ञान उन्हें केवल एआइ के छलावे से बचाएगा ही नहीं, बल्कि उन्हें एक विवेकशील नागरिक भी बनाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि वैश्विक स्तर पर एक एआइ आचार संहिता का निर्माण किया जाए, जिसमें रचनात्मक क्षेत्रों में एआइ के उपयोग की सीमाएं स्पष्ट हों। इसमें यह तय किया जाना चाहिए कि एआइ किन कार्यों में सहयोगी हो सकता है और किन कार्यों में उसे निषिद्ध किया जाए। इसके साथ ही, साहित्य, मीडिया और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों को आगे आकर जन-जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।
यह संघर्ष केवल तकनीकी नहीं, बल्कि मानवीय अस्मिता की रक्षा का संघर्ष है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि एआइ का युग हमारी सभ्यता के उस मोड़ पर खड़ा है जहां तकनीकी विकास और नैतिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन अत्यंत आवश्यक है। यदि हम इस कृत्रिमता की आंधी में सत्य, संवेदना और मौलिकता को संरक्षित नहीं रख सके, तो आनेवाली पीढिय़ां उस सत्य को पहचानने से भी वंचित रह जाएंगी, जिसे उन्होंने कभी रचा ही नहीं होगा। यह समय केवल एआइ के दुरुपयोग को रोकने का नहीं, बल्कि अपने आंतरिक मौलिक स्रोतों को पुन: जाग्रत करने का है। केवल तभी हम उस सूक्ष्म अंतर को पहचान सकेंगे, जो मशीन की नकल और मनुष्य की सजीव अनुभूति के बीच होता है।
Hindi News / Opinion / एआइ का दुरुपयोग : डिजिटल वाटरमार्किंग व मेटाडेटा टैगिंग की जरूरत
यह खबरें भी पढ़ें
लेटेस्ट ओपिनियन न्यूज़
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.