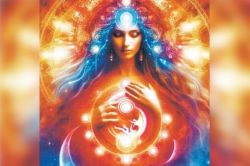अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के ऐसे प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी राय मांगने का अधिकार देता है जो सार्वजनिक महत्व के हों। लेकिन इसमें एक पेंच है- सुप्रीम कोर्ट जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान लागू होने के बाद से इस प्रावधान का केवल चौदह बार उपयोग किया गया है। कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों में बेरुबारी यूनियन केस (1960) शामिल है, जहां अदालत से पूछा गया था कि क्या भारत एक कार्यकारी समझौते के माध्यम से पाकिस्तान को क्षेत्र सौंप सकता है और राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद संदर्भ (1993), जहां राष्ट्रपति ने अदालत से यह राय मांगी थी कि क्या मस्जिद से पहले विवादित स्थल पर कोई मंदिर मौजूद था। प्रत्येक मामले में, अदालत ने सावधानी से कदम रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह पहले से तय किए गए या न्यायिक जांच के अधीन मामलों में हस्तक्षेप न करे।
अनुच्छेद 143 के तहत अदालत का क्षेत्राधिकार
अनुच्छेद 143 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को प्रदान किया गया क्षेत्राधिकार सलाहकारी प्रकृति का है, अपीलीय नहीं। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन सीमाओं को परिभाषित करता है जिनके भीतर अदालत राष्ट्रपति संदर्भ का जवाब देते समय काम कर सकती है। हालांकि अदालत के पास उसे संदर्भित मामलों पर अपनी राय देने की शक्ति है, यह उसके अपने अंतिम फैसलों को फिर से खोलने या पुनर्विचार करने तक नहीं फैलती है।
मूल मुद्दा : एक निर्णित फैसले पर पुनर्विचार?
वर्तमान संदर्भ को असामान्य बनाता है कि यह एक ऐसे प्रश्न से संबंधित है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुना दिया है। हमारी कानूनी परंपरा में, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अप्रत्यक्ष तरीकों से फिर से नहीं खोला जा सकता। अगर इस पर फिर से विचार किया जाना है, तो इसे अच्छी तरह से स्थापित नजीर के अनुसार, अदालत के ही एक बड़े बेंच के सामने रखा जाना चाहिए। यह सिर्फ एक प्रक्रियात्मक नियम नहीं है। यह न्यायिक निर्णयों में अंतिमता के संवैधानिक सिद्धांत को दर्शाता है, यह सुनिश्चित करता है कि फैसले एक बार दिए जाने के बाद राजनीतिक या संस्थागत खींचतान के अधीन न हों।
मूलभूत प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रपति संदर्भ का उपयोग सुप्रीम कोर्ट से ऐसे मामले पर राय मांगने के लिए किया जा सकता है जिस पर स्वयं अदालत ने पहले ही फैसला सुना दिया है। यह दृष्टिकोण न्यायिक घोषणाओं की अंतिमता और शक्तियों के पृथक्करण के बारे में गंभीर चिंताएं उठाता है।
कावेरी नदी विवाद में, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राज्यों के बीच जल-साझाकरण को निर्देशित करते हुए एक बाध्यकारी आदेश पारित कर दिया था। जब कार्यपालिका ने फैसले को लागू करने में हिचकिचाहट दिखाई, तो अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि उसके अंतिम फैसले बाध्यकारी और प्रवर्तनीय हैं और अनुपालन का संवैधानिक कर्तव्य विलंबकारी रणनीतियों या राजनीतिक विचारों द्वारा दरकिनार नहीं किया जा सकता। अदालत ने दोहराया कि कार्यपालिका को यह चुनने की स्वतंत्रता नहीं है कि कौन से फैसलों का पालन करना है- यह संघीय विवादों में न्यायिक प्राधिकरण का एक शक्तिशाली समर्थन है। यह सिद्धांत पूरी तरह से उन स्थितियों पर लागू होता है जहां निपटाए गए फैसलों को अनुच्छेद 143 जैसे अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से फिर से खोलने की कोशिश की जाती है।
क्या अदालत ने पहले भी ऐसे विषयों पर जिनका संविधान में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, उनकी व्याख्या की है?
हां, सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर न्याय और संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए पाठ से परे व्याख्या की है। – मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में, इसने अनुच्छेद 21 में ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ की व्याख्या उचित प्रक्रिया को शामिल करने के लिए की, जिससे जीवन के अधिकार के दायरे का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ।
- एक और प्रमुख उदाहरण न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली है। यह प्रणाली, जिसने न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को अपने सदस्यों की नियुक्ति में प्रमुख भूमिका दी, संविधान के मूल पाठ में कहीं भी नहीं मिलती, बल्कि यह पूर्णत: न्यायिक व्याख्या से विकसित हुई है।
- इंदिरा साहनी (1992) में, इसने आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा लगाई, एक ऐसा सिद्धांत जो संविधान में नहीं मिलता है लेकिन समानता और संतुलन बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है।
- केशवानंद भारती केस (1973) ने हमें बुनियादी ढांचा सिद्धांत दिया, जो संसद की संशोधन शक्तियों को सीमित करता है, भले ही अनुच्छेद 368 में ऐसी कोई पाठगत सीमा न हो।
- नवतेज सिंह जोहर (2018) में, अदालत ने अनुच्छेद 15 के तहत ‘व्यक्ति’ शब्द में ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी पहचानों को पढ़ा, यह मानते हुए कि संवैधानिक अधिकारों का गरिमा और समावेशिता के साथ विकसित होना चाहिए।
- एमसी मेहता मामलों में, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करने के लिए की गई है।
- शिक्षा का अधिकार और निजता का अधिकार अन्य आधुनिक अधिकार हैं जो अदालत द्वारा स्पष्ट पाठगत उल्लेख के बिना संवैधानिक ताने-बाने से विकसित किए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त सभी व्याख्याएं करने का मूल उद्देश्य संविधान को पुन: परिभाषित करने नहीं, बल्कि इसके मौन में जाकर हमारे संविधान निर्माताओं की संविधान रचना की गहरी समझ को आज की परिस्थितियों में इसकी भावना को संरक्षित करने के लिए है।
मेरे विचार में तमिलनाडु विधेयकों पर दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल संविधान की व्याख्या की, बल्कि उसने सहकारी संघवाद की पुष्टि भी की। इसने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को औपचारिक संस्थानों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए और संवैधानिक तंत्र को चुनावी जनादेशों का सम्मान करना चाहिए। भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेने की पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करता है। संविधान के तहत, कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट होने पर रिव्यू याचिका (अनुच्छेद 137) दायर कर सकता है और यदि रिव्यू में भी संतुष्टि न मिले, तो क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प उपलब्ध है, जैसा कि रुपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002) मामले में स्थापित हुआ। यह व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही को दर्शाती है। अनुच्छेद 143(1) के तहत, यकीनन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न पर राय मांग सकते हैं, किंतु सर्वोच्च न्यायालय कोई भी राय देने के लिए कदापि बाध्य नहीं है। यह पूर्णत: उसकी विवेकाधीन शक्ति पर निर्भर करता है कि वह किसी भी विषय पर राय देता है या नहीं, और यदि देता है, तो उसका स्वरूप क्या होगा।
(यह लेखक के अपने विचार हैं)