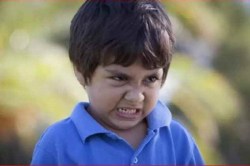बल की सुप्त अवस्था में रस का ही रूप रहता है। बल के जाग जाने पर, रस और बल भिन्न-भिन्न दिखाई देने लगते हैं। फिर भी एक-दूसरे में समाहित रहते हैं। इनका परस्पर विरुद्ध धर्म भाव में होना ही द्वैत भाव की कल्पना का आधार है। ब्रह्म में संसर्ग करके जो छोड़ दिया जाता है वह कर्म कहलाता है। यह विसर्जन ही जगत है।
परात्पर में कोई केन्द्र नहीं होता। मायाबल के उदय से इस सीमित मायापुर में एक नियमित-स्वतंत्र केन्द्र बन जाता है। एक केन्द्र होने से बलों में ग्रन्थि-बन्धन की प्रवृत्ति आ जाती है। इसी से विश्व का निर्माण होता है। शुरू में रस की प्रधानता रहती है। सृष्टि का आरंभ परमेष्ठी लोक से होता है। ब्रह्म आग्नेय प्राण रूप है। उसके मन में उठी सृष्टि कामना से प्राणों में क्षोभ पैदा होता है। प्राणों के संघर्ष से अग्नि का द्रवण होकर अप् तत्त्व उत्पन्न होता है। एक ही ब्रह्म अप् और प्राण दो भागों में बंट जाता है। मातरिश्वा वायु द्वारा अप् रूप रेत की आहुति अग्नि में होती है। इसी से विराट् उत्पन्न होता है।
अप् का अर्थ प्राचीन मत के अनुसार ‘कर्म’ है। मातरिश्वा सूत्रवायु है। सूत्रवायु यजु: के ‘जू’ भाग (विद्या रूप स्थिति) में कर्म का आधान करता है। अप् (कर्म) आहुति द्रव्य है। मातरिश्वा द्वारा इस आहुति से अव्यय पुरुष यज्ञ रूप हो जाता है। अग्नि-सोमात्मक यज्ञ। यज्ञ से सृष्टि होती है। यजु:- अनेजदेजत् है अर्थात् वह परमात्म तत्त्व है- स्थिति और गति रूप है। रेत का स्थिर भाग मातरिश्वा द्वारा कर्म रूप में आधान किया जाता है। सूक्ष्म भाव स्थूल में रूपान्तरित हो जाता है। अब यह माता की वस्तु बन जाता है। मातरिश्वा द्वारा आधान होने पर आत्मा रूप योनि तथा आपोमय रेत के संसर्ग से अप् समूह में परस्पर ग्रन्थि पड़ जाती है। यही जनन रूप सृष्टि है।
रस और बल ही क्रमश: अमृत और मृत्यु ही कहे जाते हैं। मृत्यु अमृत में लीन हो जाती है, अत: अमृत को लिंग कहा जाता है। कार्य रूप मृत्यु अमृत में मिलती है अत: कर्म को योनि कहते हैं। रस और बल में बल ही रस से सम्बन्ध जोड़ता है। रस, बल से सम्बद्ध नहीं होता। रस के आधार पर ही बल की स्वरूप सत्ता बनती है। रस के बिना बल का कोई स्वरूप नहीं है।
रस और बल का योग संसर्ग कहलाता है। इसकी प्रधानता से स्वरूप संसर्ग तथा बल की प्रधानता से वृत्तिता संसर्ग कहा जाता है। स्वरूप संसर्ग में रस और बल के विभूति-योग-बन्ध रूप बनते हैं। वृत्तिता में रस-बल के अतिरिक्त अन्य बलों का योग होने से शक्ति रूपा बलों का संसर्ग सृष्टि क्रम को स्थूलता और गति प्रदान करते हैं। जीव के ग्रन्थि-बन्धन जल में लहर पैदा करने तथा बुद्बुद् स्वरूप जैसा है। शरीर पृथ्वी है- पंच महाभूतों का निर्माण है। जैसे जल से आठ स्तरों पर पृथ्वी निर्मित होती है, उसी प्रकार मात्रा और छन्द के सिद्धान्त से गर्भस्थ जीव की देह का निर्माण होता है। जीव भाग मात्रा तथा शरीर छन्द का वाचक बनता है। स्वरूप संसर्ग के विभूति-योग-बन्ध से ही आत्मा के मन-प्राण-वाक् का स्वरूप बनता है। इसी प्रकार वृत्तिता संसर्ग के उदार, समवाय, आसक्ति भाव से नाम-रूप-कर्म बनते हैं। स्वरूप संसर्ग युक्त बल को भाव कहते हैं। वृत्तिता संसर्ग युक्त बल को कर्म कहा जाता है।
रस सत्ता-आनन्द-चेतना है, सदा एक भाव में ही रहता है। आत्मा मन-प्राण-वाक् रूप कहा है। मन ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, कामना है। श्वोवसीयस मन का सृष्टि भाग है। मन की कामना का पोषण दो रूप में ही होता है। एक, प्राणरूप में तथा दूसरा, वाक् रूप में। प्राण रूप भी स्पन्दन है- ध्वनि है- मंत्र है- शब्द ब्रह्म है, सरस्वती है। वाक् रूप पदार्थ है- अन्न है- ब्रह्म है। लक्ष्मी या मैटर है। अर्थात् कामना भी पदार्थ और ऊर्जा के बाहर की नहीं होती। दोनों रूप भी वाक् के ही हैं। प्राणमय और अन्नमय दो ही कोश स्थूल सृष्टि से सम्बन्ध रखते हैं। नाम-रूप-कर्म की सृष्टि ही शक्ति-प्रकृति-स्वभाव का क्षेत्र है।
जीव का आना स्वरूप संसर्ग है, निर्माण और संचालन वृत्तिता संसर्ग। एक में ब्रह्म-माया है- एक में शक्ति की भूमिका। सृष्टि युगल तत्त्वों से दो भागों में ही होती है। एक प्राण सृष्टि और दूसरी पदार्थ सृष्टि। गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जो व्याख्या है- वह इन्हीं दो सृष्टि स्वरूपों की है-
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते।
एतद्यो वेत्ति तं प्राहु: क्षेत्रज्ञ इति तद्विद:।। (गीता १३.१) शरीर क्षेत्र है (पदार्थ है), आत्मा क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा) है। अर्थात् जीव जब शरीर में (गर्भ) आता है, तब उसके दो भिन्न-भिन्न धरातल पर प्रक्रिया होती है। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर का अंग होता है तथा शरीर स्थूल सृष्टि का।
प्रकृति स्पष्ट भी है, निर्मल भी है और मर्यादा के बाहर कभी जाती भी नहीं है। उदाहरण के लिए मां प्रकृति है। त्रिगुणात्मक भी है और पुरुष की पूरक भी बनी रहती है। पुरुष के लिए सन्तान प्राप्त करने उसके पास आती है। सन्तान अथवा जीवात्मा परा प्रकृति है। उसे अपने परा स्वरूप में धारण करती है। कोई इस बात की कल्पना करके तो देखे। स्थूल शरीर में सूक्ष्म स्तर तक उठना, जीवात्मा का ग्रहण करके पुन: स्थूल शरीर में लौट आना। पुरुष को तो भनक तक नहीं लग पाती। उसकी पहुंच तो अपरा प्रकृति के कार्यों तक ही सीमित रहती है।
पुरुष के पास से क्या प्राप्त हुआ- स्त्री को। मायाविशिष्ट रस। यह रस मार्ग बदलता हुआ अपने गन्तव्य तक पहुंचता है। मार्ग का और जीव का यह वृत्तिता सम्बन्ध कहा जाता है। जीव की इस यात्रा से मार्ग का कुछ नहीं बदला। किन्तु अन्य बल भी मार्ग में जुड़ते गए। जीव के अन्न अथवा भोज्य पदार्थों का सर्जन करने के लिए- मार्ग में- उसे शक्ति कहते हैं, प्रकृति या स्वभाव कहते हैं। मायाबल युक्त रस में प्रवाह रूप जिस बल का सम्बन्ध होता है (वृत्तिता) वह शक्ति है। वह रस-बल से अतिरिक्त है। शक्ति के द्वारा जो भोज्य पदार्थ तैयार होता है, वह अर्थ जात पुरुषार्थ कहलाता है।
मां की दिव्यता को यहां समझा जा सकता है। वह सूक्ष्म धरातल पर जीव से परिचय करती है, उसे संस्कारित करती है। अपने अक्षर शरीर से। स्थूल से यह सम्पर्क नहीं हो सकता। माता यदि अनभिज्ञ है, तो सन्तान संस्कारित नहीं होगी। जीव जिस शरीर को छोड़कर आया, वैसा ही नई देह में अगले सौ साल पूरे करेगा। जीव के शरीर का निर्माण पदार्थ (जड़) या पशु रूप है जिसमें मूल आधार अन्न, आहार-विहार है। यह अन्न-ब्रह्म का क्षेत्र है। जीव का निर्माण सूक्ष्म स्तर पर शब्द-ब्रह्म का क्षेत्र है, जिसका आधार सूक्ष्म में मां द्वारा प्रदत्त ज्ञान होता है। यही स्त्री की पूर्णता का आधार है।
क्रमश:
gulabkothari@epatrika.com